बचपन मेरी ज़िंदगी से तो निकल गया था, मगर बचपन दिल से नहीं निकला था- जिसकी वजह से दिनभर मां की टोका-टाकी झेलनी पड़ रही थी। खुल कर हंस भी लेती तो मां की टोक उसे सांप की तरह डसती थी- “गुड्डी, न जाने तेरा बचपना कब जाएगा, यह सब ससुराल में तो नहीं चलेगा।” कभी दिन में देर तक सोई रहती तो भी यही कटु वाक्य मुझे झिंझोड़ कर जगाया करता था- ‘गुड्डी  सूरज निकल आया है, तू है कि घोड़े बेच कर सो रही है। यह सब ससुराल में नहीं चलेगा।’ मां ने टोक-टोक कर ससुराल शब्द को जैसे मेरे लिए तिहाड़ जेल का पर्यायवाची बना डाला था। ससुराल में यह नहीं चलेगा- ससुराल में वो नहीं चलेगा सुन-सुन कर मेरे कान पक गए थे। मां की इस वाक्य की लाठी ने ही मेरे दिल से भी बचपना खदेड़ कर अतीत की किसी गहरी खाई में फेंक दिया था। मुझमें ऐसे धीरे-धीरे परिवर्तन आया कि कब गुड्डी को बचपना अपने साथ ले गया पता ही नहीं चला। खुल कर मौज़-मस्ती करने वाली, ठहाके लगाने वाली मेरे दिल के भीतर की गुड्डी अचानक ही कहीं खो गई तो किशोरी के रूप में कविता बनी खड़ी मैं खुद ही आईने में देख-देख कर आश्चर्य करती। यौवन ने मेरी देह में प्रवेश किया मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मैं खुद में ही खोई हुई थी। गुमसुम सी, खोई-खोई, ठगी-ठगी सी कविता को मां की टोक ने फिर झिंझोड़ा- “कविता यह तुम कहां खोई रहती हो? यही दिन हैं, जी भर कर सबकुछ सीख ले ससुराल में काम आएगा।” बस फिर क्या था मां के साथ-साथ बड़ी जीजी भी जैसे मुझे सबकुछ सिखाने पर आमादा हो गई थी। अपनी प्यारी बचपन की मूक सखी को कम से कम एक बार मैं फिर भी ट्रंक से निकाल कर देखना नहीं भूलती थी। मगर जब मेरी शादी पक्की हुई तो मेरा ध्यान जैसे बचपन से हट गया था। अब जब मेरा दांव लगता मैं उनकी तसवीर पर एक नज़र डाल आती। वो तसवीर ही जैसे मेरे दिल में उतरी और मेरे वजूद पर छा गई। बाबुल की गुड्डी अब अपने पिया की कविता बन चुकी थी। एक अजनबी होकर भी जब इन्होंने एक मित्र जैसा सलूक किया तो पहली बार जैसे ससुराल शब्द के प्रति मेरे अंदर एक नई उत्सुकता जागी थी। ससुराल आकर पता चला था कि ससुराल एक जेल न होकर भले ही एक नई और रंगीन दुनिया है मगर मेरी स्थिति फिर भी वहां किसी खुले क़ैदी से अधिक कुछ नहीं थी।
सूरज निकल आया है, तू है कि घोड़े बेच कर सो रही है। यह सब ससुराल में नहीं चलेगा।’ मां ने टोक-टोक कर ससुराल शब्द को जैसे मेरे लिए तिहाड़ जेल का पर्यायवाची बना डाला था। ससुराल में यह नहीं चलेगा- ससुराल में वो नहीं चलेगा सुन-सुन कर मेरे कान पक गए थे। मां की इस वाक्य की लाठी ने ही मेरे दिल से भी बचपना खदेड़ कर अतीत की किसी गहरी खाई में फेंक दिया था। मुझमें ऐसे धीरे-धीरे परिवर्तन आया कि कब गुड्डी को बचपना अपने साथ ले गया पता ही नहीं चला। खुल कर मौज़-मस्ती करने वाली, ठहाके लगाने वाली मेरे दिल के भीतर की गुड्डी अचानक ही कहीं खो गई तो किशोरी के रूप में कविता बनी खड़ी मैं खुद ही आईने में देख-देख कर आश्चर्य करती। यौवन ने मेरी देह में प्रवेश किया मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मैं खुद में ही खोई हुई थी। गुमसुम सी, खोई-खोई, ठगी-ठगी सी कविता को मां की टोक ने फिर झिंझोड़ा- “कविता यह तुम कहां खोई रहती हो? यही दिन हैं, जी भर कर सबकुछ सीख ले ससुराल में काम आएगा।” बस फिर क्या था मां के साथ-साथ बड़ी जीजी भी जैसे मुझे सबकुछ सिखाने पर आमादा हो गई थी। अपनी प्यारी बचपन की मूक सखी को कम से कम एक बार मैं फिर भी ट्रंक से निकाल कर देखना नहीं भूलती थी। मगर जब मेरी शादी पक्की हुई तो मेरा ध्यान जैसे बचपन से हट गया था। अब जब मेरा दांव लगता मैं उनकी तसवीर पर एक नज़र डाल आती। वो तसवीर ही जैसे मेरे दिल में उतरी और मेरे वजूद पर छा गई। बाबुल की गुड्डी अब अपने पिया की कविता बन चुकी थी। एक अजनबी होकर भी जब इन्होंने एक मित्र जैसा सलूक किया तो पहली बार जैसे ससुराल शब्द के प्रति मेरे अंदर एक नई उत्सुकता जागी थी। ससुराल आकर पता चला था कि ससुराल एक जेल न होकर भले ही एक नई और रंगीन दुनिया है मगर मेरी स्थिति फिर भी वहां किसी खुले क़ैदी से अधिक कुछ नहीं थी।
यह ससुराल वालों का एक सहज-सा भय था कि मेरे स्कूल में भी बहू होने का एहसास मेरे वजूद पर छाया रहता था। कई बार मेरे स्टाफ़ का कोई सदस्य मुझे मैडम कह कर पुकारता तो मैं भय से चौंक जाया करती थी। मैडम होने का एहसास जागृत होते ही मेरे आतंकित चेहरे पर एक मलीन सी मुस्कान खिल जाती। न जाने मेरे मन में क्या आया था कि मैंने पूरे स्टाफ़ के साथ मीटिंग की और उनके लिए भी स्कूल ड्रैस में आना अनिवार्य कर दिया। बहुओं सा अनुशासन ओढ़े वे सब मेरे निर्णय से सहमत न होते हुए भी चुप थे। एक विजयी-सा एहसास मेरे भीतर तक सुखदानुभूति सा पसर गया। वाइस प्रिंसीपल कुनिका ने एक सवाल हवा में उछाला- “मैडम क्या आप भी ड्रैस में आया करेंगी?” इस सवाल के साथ बैठक तो ख़त्म हो गई मगर मेरे भीतर एक उथल-पुथल शुरू हो गई। हवा में उछले सवाल में जैसे उनका जवाब भी छुपा हुआ था। बहू होने के एहसास को स्कूल के दौरान मैं वर्दी से ढक लेना जाहती थी। अन्ततः सभी के भीतरी संकोच में मेरा भी संकोच शामिल हो गया तो स्टाफ़ के लिए यूनिफार्म की जगह उसके प्रतीक रूप में एक जैकेट पहनना अनिवार्य कर दिया जिस पर स्कूल का प्रतीक चिन्ह उकरा हुआ हो। स्कूल में प्रवेश करते ही सभी अपनी-अपनी जैकेट पहन लेतीं। जब मैंने पहली बार जैकेट पहनी तो यूं लगा था मानों गुड्डी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही हो। जब मैं गुड्डी थी तो ज़िंदगी मानों एक खेल था- एक मौज़ और मस्ती। सारा दिन धमाल गुड्डे-गुड़ियों के खेल इतने रोचक होते थे कि मासूम बचपन भविष्य के तमाम रिश्तों को ओढ़ कर आनन्दित हो लिया करता था। हमेशा मुझे कर्कश सास की भूमिका ही मिला करती थी और न चाहते हुए भी मुझे बुरी भूमिका निभानी पड़ती थी। बड़ी जीजी न जाने क्यों सदैव पापा की भूमिका ही निभाया करती थी। हाथ के गुड्डे-गुड़ियां कब हाथ से छूट गए कुछ याद नहीं पड़ता। डोली में बैठकर मायके से विदा होकर जो ससुराल में क़दम रखा तो यूं लगा जैसे कि कविता नहीं मैं, मेरी जगह  कोई चाबी से चलने वाली गुड़िया थी। रोज़ अम्मा उसे अपने मन माने ढंग से सजातीं और अपने नातेदारों, सगे-सम्बन्धियों और पास-पड़ोसियों को दिखा कर मुंह दिखाई उगाहने लगी थीं और पहले ही दिन सुहागरात की सेज पर भी गुड़िया से नया खेल-खेला गया। ससुराल वालों के लिए मैं एक खिलौना बन गई थी, जिसे वो अपने परिवार के सुख व समृद्धि के लिए मेरे पापा से मांग लाए थे। ज़िंदगी ने ऐसा खेल खेला था कि मैं बेटी से किसी की बहू बन गई थी। मंगलसूत्र से बंधी और लाल बिन्दिया के पीछे छुपी वो गुड्डी ससुराल वालों के लिए रिमोट से चलने लगी। शिक्षित परिवार है मगर पारंपरिक भी। जब बाबू जी ने मुझे स्कूल की प्रिंसीपल बनाने का निर्णय लिया तो ऐसा लगा कि बहू होने के साथ-साथ कहीं मैं कुछ और भी हो सकती हूं। कुछ दिन तो लगा कि इन दो मुखौटों की अलग-अलग भूमिकाएं निभाने की क्षमता मुझमें नहीं है। प्रिंसीपल पर बाबू जी की बहू और घर में बाबू जी की बहू पर प्रिंसीपल मैडम कुछ हद तक हावी रही। दोनों को एक दूसरे से नितांत दूर रखना ही जैसे मेरे लिए सिरदर्दी बन गया था। बड़ी जद्दोजेहद के बाद मैं दोनों को एक-दूसरे से अलग कर पाई थी। ऐसा होने के बाद मुझे लगा कि प्रिंसीपल मैडम होकर मुझे स्कूल में रहना अच्छा लगने लगा है। अपने स्कूल में आते ही मैं जैसे ज़िन्दा हो उठती हूं। यूनिफार्म में मैं जब युवतियों को देखती हूं तो उनमें से मैं गुड्डी को ढूंढ़ने लगती हूं। अभी उसी दिन छोटी सी बात ने मुझे भावाकुल किए रखा। प्लॅस वन की एक छात्रा क्लास में अपने बचपन की गुड़िया ले आई सखियों को दिखाने। क्लास टीचर ने उसे पकड़ा, मेरे कमरे में ले आई। उसकी गुड्डी मेरे टेबल पर रख दी। ऋतु शर्म से दोहरी हुई जा रही थी। मैंने उसकी मैडम को उसे वहीं छोड़ कर चले जाने के लिए कहा। मैडम के जाते ही वो, “सॉरी मैम”, की अनुनय विनय करने लगी थी। “ऋतु, तुम्हारी डॉल तो बहुत स्मार्ट है भई, नो सॉरी,
कोई चाबी से चलने वाली गुड़िया थी। रोज़ अम्मा उसे अपने मन माने ढंग से सजातीं और अपने नातेदारों, सगे-सम्बन्धियों और पास-पड़ोसियों को दिखा कर मुंह दिखाई उगाहने लगी थीं और पहले ही दिन सुहागरात की सेज पर भी गुड़िया से नया खेल-खेला गया। ससुराल वालों के लिए मैं एक खिलौना बन गई थी, जिसे वो अपने परिवार के सुख व समृद्धि के लिए मेरे पापा से मांग लाए थे। ज़िंदगी ने ऐसा खेल खेला था कि मैं बेटी से किसी की बहू बन गई थी। मंगलसूत्र से बंधी और लाल बिन्दिया के पीछे छुपी वो गुड्डी ससुराल वालों के लिए रिमोट से चलने लगी। शिक्षित परिवार है मगर पारंपरिक भी। जब बाबू जी ने मुझे स्कूल की प्रिंसीपल बनाने का निर्णय लिया तो ऐसा लगा कि बहू होने के साथ-साथ कहीं मैं कुछ और भी हो सकती हूं। कुछ दिन तो लगा कि इन दो मुखौटों की अलग-अलग भूमिकाएं निभाने की क्षमता मुझमें नहीं है। प्रिंसीपल पर बाबू जी की बहू और घर में बाबू जी की बहू पर प्रिंसीपल मैडम कुछ हद तक हावी रही। दोनों को एक दूसरे से नितांत दूर रखना ही जैसे मेरे लिए सिरदर्दी बन गया था। बड़ी जद्दोजेहद के बाद मैं दोनों को एक-दूसरे से अलग कर पाई थी। ऐसा होने के बाद मुझे लगा कि प्रिंसीपल मैडम होकर मुझे स्कूल में रहना अच्छा लगने लगा है। अपने स्कूल में आते ही मैं जैसे ज़िन्दा हो उठती हूं। यूनिफार्म में मैं जब युवतियों को देखती हूं तो उनमें से मैं गुड्डी को ढूंढ़ने लगती हूं। अभी उसी दिन छोटी सी बात ने मुझे भावाकुल किए रखा। प्लॅस वन की एक छात्रा क्लास में अपने बचपन की गुड़िया ले आई सखियों को दिखाने। क्लास टीचर ने उसे पकड़ा, मेरे कमरे में ले आई। उसकी गुड्डी मेरे टेबल पर रख दी। ऋतु शर्म से दोहरी हुई जा रही थी। मैंने उसकी मैडम को उसे वहीं छोड़ कर चले जाने के लिए कहा। मैडम के जाते ही वो, “सॉरी मैम”, की अनुनय विनय करने लगी थी। “ऋतु, तुम्हारी डॉल तो बहुत स्मार्ट है भई, नो सॉरी, 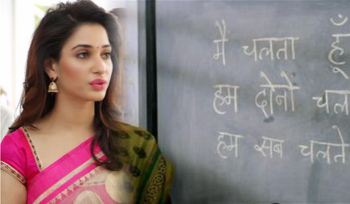 इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।” मैंने उसे अपने निकट बुलाया, उसकी रुलाई जैसे छूटने को थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया तो पसीने से भीगा सा लगा। मेरे हाथ के स्पर्श से वो कुछ आश्वस्त हुई तो वो बोली कि वो अपनी गुड्डी से बहुत प्यार करती है। मैंने उसे दोबारा स्कूल में न लाने की सलाह देते हुए जब कहा कि उसकी मूक सहेली को यूं अपमान सहना पड़ता है। वो अपनी डॉल को लेकर कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही मुझे अपनी आंखें भी गीली-सी जान पड़ी। ऋतु बचपन की उंगली को कसकर पकड़े थी और किशोरावस्था उसका उससे साथ छुड़ाने को आमादा थी। मेरा भी मन चाहा था कि मैं अपने बचपन में लौट जाऊं और पुनः कविता से गुड्डी बन जाऊं। मुझे अपनी सारी छात्राएं अब गुड्डी की तरह दिखने लगी थीं। एक ख़्याल अचानक आया कि स्कूल में डॉल प्रतियोगिता करवाऊं। दिल यह सोच कर बल्लियों उछल पड़ा। दूसरे ही दिन सुबह प्रार्थना सभा में मैंने घोषणा करवा दी कि अपने अपने बचपन के खेल-खिलौनों में से गुड्डे-गुड़ियां लाकर प्रदर्शनी में रखो व पुरस्कार जीतो। भीड़ में खड़ी ऋतु के चेहरे पर ग़ज़ब का उल्लास था। दूसरे ही दिन मेरे रूम में सुन्दर-सुन्दर डॉल्ज़ आकर एकत्रित होने लगी। देखते ही देखते मेरा प्रिंसीपल वाला कमरा डॉल म्यूज़ियम बन गया था। मेरे मायके से मैंने भी एक डॉल कोरियर से मंगवा ली थी। मेरी प्रेरणा से मेरे स्टाफ़ को भी लगा कि उन्हें भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। मेरे हाथों में मेरा बचपन था और दिल में उतर आया था मेरा बचपना। मैंने उसे पूरी भावातिरेक से स्पर्श किया उसे लगातार सहलाया तो मेरी आंखों में जमा बचपन जैसे मोम की तरह जल कर बूंद-बूंद पिघलने लगा था। मैंने जल्दी से आंखें पोंछ लीं और दीवार पर लगे अपने व्हाईट-बोर्ड पर नज़र टिकाई। बोर्ड पर कुछ नहीं लिखा था। मैं अपने आंसुओं से उस पर लिखने लगी थी कि मेरे बचपन तू आ आ, जवानी को ले जा! मैंने उस पर बार-बार लिखा, मगर कोई पढ़ नहीं पाएगा शायद। प्रतियोगिता के निर्णय में ऋतु की गुड़िया को मैंने प्रथम पुरस्कार दे दिया था क्योंकि उसने मुझ कविता को मेरी खोई हुई गुड्डी से जो मिलवाया था। सभी लड़कियां अपनी अपनी गुड्डियों को प्रतियोगिता के बाद मेरे कमरे से वापिस ले गई थीं
इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।” मैंने उसे अपने निकट बुलाया, उसकी रुलाई जैसे छूटने को थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया तो पसीने से भीगा सा लगा। मेरे हाथ के स्पर्श से वो कुछ आश्वस्त हुई तो वो बोली कि वो अपनी गुड्डी से बहुत प्यार करती है। मैंने उसे दोबारा स्कूल में न लाने की सलाह देते हुए जब कहा कि उसकी मूक सहेली को यूं अपमान सहना पड़ता है। वो अपनी डॉल को लेकर कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही मुझे अपनी आंखें भी गीली-सी जान पड़ी। ऋतु बचपन की उंगली को कसकर पकड़े थी और किशोरावस्था उसका उससे साथ छुड़ाने को आमादा थी। मेरा भी मन चाहा था कि मैं अपने बचपन में लौट जाऊं और पुनः कविता से गुड्डी बन जाऊं। मुझे अपनी सारी छात्राएं अब गुड्डी की तरह दिखने लगी थीं। एक ख़्याल अचानक आया कि स्कूल में डॉल प्रतियोगिता करवाऊं। दिल यह सोच कर बल्लियों उछल पड़ा। दूसरे ही दिन सुबह प्रार्थना सभा में मैंने घोषणा करवा दी कि अपने अपने बचपन के खेल-खिलौनों में से गुड्डे-गुड़ियां लाकर प्रदर्शनी में रखो व पुरस्कार जीतो। भीड़ में खड़ी ऋतु के चेहरे पर ग़ज़ब का उल्लास था। दूसरे ही दिन मेरे रूम में सुन्दर-सुन्दर डॉल्ज़ आकर एकत्रित होने लगी। देखते ही देखते मेरा प्रिंसीपल वाला कमरा डॉल म्यूज़ियम बन गया था। मेरे मायके से मैंने भी एक डॉल कोरियर से मंगवा ली थी। मेरी प्रेरणा से मेरे स्टाफ़ को भी लगा कि उन्हें भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। मेरे हाथों में मेरा बचपन था और दिल में उतर आया था मेरा बचपना। मैंने उसे पूरी भावातिरेक से स्पर्श किया उसे लगातार सहलाया तो मेरी आंखों में जमा बचपन जैसे मोम की तरह जल कर बूंद-बूंद पिघलने लगा था। मैंने जल्दी से आंखें पोंछ लीं और दीवार पर लगे अपने व्हाईट-बोर्ड पर नज़र टिकाई। बोर्ड पर कुछ नहीं लिखा था। मैं अपने आंसुओं से उस पर लिखने लगी थी कि मेरे बचपन तू आ आ, जवानी को ले जा! मैंने उस पर बार-बार लिखा, मगर कोई पढ़ नहीं पाएगा शायद। प्रतियोगिता के निर्णय में ऋतु की गुड़िया को मैंने प्रथम पुरस्कार दे दिया था क्योंकि उसने मुझ कविता को मेरी खोई हुई गुड्डी से जो मिलवाया था। सभी लड़कियां अपनी अपनी गुड्डियों को प्रतियोगिता के बाद मेरे कमरे से वापिस ले गई थीं  मगर मेरे कमरे में मेरी गुड्डी अब भी पड़ी थी। मैं उसे रोज़ देखती हूं, स्पर्श करती हूं और अकेले में उससे बातें भी करती हूं- वह मेरी अन्तरंग सखी बन गई। बेझिझक मैं उसे अपने पति की शिकायत भी कर लेती हूं और अम्मा जी से मिले उलाहने भी उसी की झोली में डाल देती हूं। गर्मी की छुट्टियां होने वाली हैं। मैं उसे अपने साथ इलाहाबाद ले जाऊंगी, वहां से लौटूंगी तो इस में प्राणों का संचार भी हो चुका होगा। अपने रक्त और सांस के साथ जोड़ कर उसे अपनी कोख में लाऊंगी और इसे नया जन्म दूंगी। प्यार से लाड़ से अपने चाव भरे मल्हार से उसे पालूंगी। अपना दूध पिलाकर, अपना बचपन इसे उपहार देकर उसमें रही कमियों को दूर करके। यह सोच कर मैं अपनी गुड्डी को उठाती हूं और स्कूल की माई को उसे अपनी कार में रखने का आदेश देती हूं। गर्मियों की छुट्टियां कल से शुरू हो रही हैं मगर मेरा मन अभी इलाहाबाद की गाड़ी पकड़ने को भाग रहा है।
मगर मेरे कमरे में मेरी गुड्डी अब भी पड़ी थी। मैं उसे रोज़ देखती हूं, स्पर्श करती हूं और अकेले में उससे बातें भी करती हूं- वह मेरी अन्तरंग सखी बन गई। बेझिझक मैं उसे अपने पति की शिकायत भी कर लेती हूं और अम्मा जी से मिले उलाहने भी उसी की झोली में डाल देती हूं। गर्मी की छुट्टियां होने वाली हैं। मैं उसे अपने साथ इलाहाबाद ले जाऊंगी, वहां से लौटूंगी तो इस में प्राणों का संचार भी हो चुका होगा। अपने रक्त और सांस के साथ जोड़ कर उसे अपनी कोख में लाऊंगी और इसे नया जन्म दूंगी। प्यार से लाड़ से अपने चाव भरे मल्हार से उसे पालूंगी। अपना दूध पिलाकर, अपना बचपन इसे उपहार देकर उसमें रही कमियों को दूर करके। यह सोच कर मैं अपनी गुड्डी को उठाती हूं और स्कूल की माई को उसे अपनी कार में रखने का आदेश देती हूं। गर्मियों की छुट्टियां कल से शुरू हो रही हैं मगर मेरा मन अभी इलाहाबाद की गाड़ी पकड़ने को भाग रहा है।
